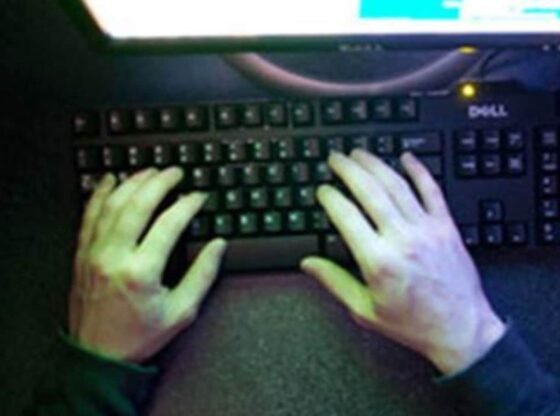24 अक्टूबर, 2025 05:00 अपराह्न IST
पहली बार प्रकाशित: 24 अक्टूबर, 2025, शाम 05:00 बजे IST
भारत अपने डिजिटल विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने एआई-जनित वीडियो, छवियों और आवाजों सहित सिंथेटिक सामग्री को विनियमित करने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा प्रस्तावित किया है। 6 नवंबर तक सार्वजनिक परामर्श के लिए खुले इस मसौदे का उद्देश्य ऐसी सामग्री बनाने वाले रचनाकारों और प्लेटफार्मों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है।
यदि इसे अपनाया जाता है, तो भारत एआई-संचालित गलत सूचना के खतरों को औपचारिक रूप से संबोधित करने वाले पहले लोकतंत्रों में से एक बन जाएगा। एक साल में जब डीपफेक ने राजनीति में घुसपैठ कर ली हैमनोरंजन और सामाजिक प्रवचन, समय अधिक जरूरी नहीं हो सकता है।
दांव पर डेटा या गोपनीयता से कहीं अधिक गहरा कुछ है; यह स्वयं सत्य की अखंडता है।
मसौदा संशोधन निम्नलिखित का प्रस्ताव करेगा। एक, “कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी” को प्रामाणिक मीडिया जैसा दिखने के लिए एल्गोरिदम द्वारा बनाई या बदली गई सामग्री के रूप में परिभाषित करना। दो, उन्हें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता होती है जो ऐसी सामग्री को स्पष्ट रूप से लेबल करने के लिए बनाते या होस्ट करते हैं, उदाहरण के लिए, दृश्य स्थान का कम से कम 10 प्रतिशत या ऑडियो का पहला 10 प्रतिशत अस्वीकरण के लिए समर्पित करना। तीन, वे सिंथेटिक मीडिया अपलोड के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली और उपयोगकर्ता घोषणाओं को अनिवार्य करते हैं। और चार, वे हानिकारक सिंथेटिक सामग्री को हटाने वाले बिचौलियों के लिए सुरक्षित आश्रय सुरक्षा बनाए रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करने वालों को दंडित करते हैं।
सरकार का लक्ष्य प्रतिरूपण, फर्जी समाचार आदि के प्रसार पर अंकुश लगाना है डीपफेक-आधारित धोखाधड़ी नवीनता को दबाए बिना। लेकिन उस इरादे को प्रभावी कार्यान्वयन में तब्दील करना भारत की सबसे कठिन शासन चुनौती होगी।
प्रत्येक तकनीकी क्रांति समाज की प्रतिरक्षा प्रणाली का परीक्षण करती है। इंटरनेट ने गोपनीयता का परीक्षण किया; सोशल मीडिया ने परखी सभ्यता; एआई अब स्वयं वास्तविकता का परीक्षण कर रहा है। डीपफेक टूल रचनाकारों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बना सकते हैं। एक छोटा व्यवसाय बहुभाषी विज्ञापन बनाने के लिए AI का उपयोग कर सकता है; एक फिल्म निर्माता खोई हुई फ़ुटेज को पुनर्स्थापित कर सकता है। लेकिन वही तकनीक प्रतिष्ठा को नष्ट भी कर सकती है, चुनावों में हेरफेर कर सकती है या हिंसा भड़का सकती है।
विरोधाभास यह है: हमें विकास के लिए एआई की आवश्यकता है, लेकिन हमें विश्वास के लिए शासन की आवश्यकता है। MeitY के मसौदा नियम इस बात की मान्यता है कि सच्चाई केवल एक नैतिक समस्या नहीं, बल्कि एक बुनियादी ढांचा समस्या बन गई है। सवाल यह है कि रचनात्मकता को प्रभावित किए बिना उस बुनियादी ढांचे का निर्माण कैसे किया जाए।
भारत को अपनी क्षमता से अधिक तेजी से कानून बनाने के प्रलोभन से बचना चाहिए। मसौदे का प्रस्तावित “10 प्रतिशत दृश्य अस्वीकरण” प्रतीकात्मक रूप से मजबूत है लेकिन तकनीकी रूप से कमजोर है। अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण तीन स्तंभों पर टिका होगा। सबसे पहले, सत्यापन बुनियादी ढाँचा: प्रामाणिकता के लिए आधार के समान एक डिजिटल उद्गम ढाँचा बनाएँ, जहाँ सामग्री के प्रत्येक टुकड़े पर एक अदृश्य लेकिन सत्यापन योग्य हस्ताक्षर हो। दूसरा, स्तरीय जवाबदेही: सिंथेटिक मीडिया की मेजबानी, निर्माण या मुद्रीकरण करने वाले प्लेटफार्मों के बीच अंतर करें। प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए. तीसरा, एआई साक्षरता: नागरिकों को हेरफेर का पता लगाने के लिए तैयार करना। अकेले प्रौद्योगिकी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती; जागरूक नागरिक कर सकते हैं।
ऐसी प्रणाली भारत को न केवल आज्ञाकारी बनाएगी, बल्कि प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी। नवप्रवर्तन को सत्यनिष्ठा के साथ संतुलित करने का एक मॉडल।
वैश्विक स्तर पर नियामक इसी दुविधा से जूझ रहे हैं। EU का AI अधिनियम सिंथेटिक सामग्री की वॉटरमार्किंग को अनिवार्य करता है। अमेरिका स्वैच्छिक कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं पर निर्भर है। चीन को “डीप सिंथेसिस” मीडिया के लिए सरकारी पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता है।
भारत की चुनौती अनोखी है. इसकी डिजिटल आबादी विशाल, बहुभाषी है और समाचारों के लिए सोशल मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए वायरल गलत सूचना का जोखिम तेजी से अधिक है। इसलिए भारत को तीसरा रास्ता अपनाना होगा। न तो अहस्तक्षेप सिलिकॉन वैली और न ही राज्य-नियंत्रित बीजिंग। एक मॉडल जो रचनाकारों को सशक्त बनाता है, उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करता है और जवाबदेही लागू करता है।
लोकतंत्र विश्वास पर चलता है. और जब सत्य तरल हो जाता है तो विश्वास नाजुक होता है। किसी उम्मीदवार का हेरफेर किया गया वीडियो, किसी पत्रकार की क्लोन की गई आवाज़, या कोई जाली सरकारी आदेश किसी भी तथ्य-जाँच की तुलना में जनता के विश्वास को तेज़ी से कमज़ोर कर सकता है।
समाधान सेंसरशिप नहीं है. यह स्पष्टता है. प्रामाणिकता को विनियमित करें, राय को नहीं। यदि भारत एआई-जनित मीडिया में पारदर्शिता को संस्थागत बना सकता है, तो यह न केवल अपने चुनावों की रक्षा करेगा। यह दुनिया के लिए डिजिटल जिम्मेदारी का एक मॉडल निर्यात करेगा।
आने वाले महीने तय करेंगे कि भारत विश्वास का ढांचा तैयार करेगा या डर की नौकरशाही का। सरकार को स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और नागरिक समाज समूहों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमन नवाचार को दबाने के बजाय उसका मार्गदर्शन करे। यह अकेले डीपफेक के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रामाणिकता की लड़ाई है। भारत के पास नैतिक एआई प्रशासन में दुनिया का नेतृत्व करने का पीढ़ी में एक बार आने वाला अवसर है। वही देश जिसने पहचान सत्यापित करने के लिए आधार बनाया, अब सत्य की पुष्टि के लिए रेल बना सकता है। क्योंकि हमारे युग की चुनौती फेक न्यूज़ नहीं है। यह नकली हकीकत है. और समाधान डर नहीं है. यह भरोसा है.
एआई के युग में भरोसा सबसे बड़ी खाई होगी।
लेखक ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख हैं